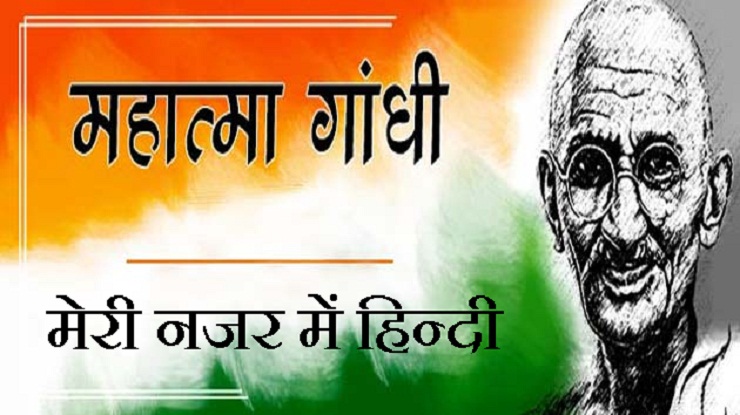प्रो. विनोद कुमार मिश्र
महासचिव
विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी ऐसे इकलौते राष्ट्रनायक बने जिन्होंने अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध पूरे देश का आह्वान किया और आह्वान की धारदार भाषा के रूप में हिंदी की पहचान की। उन्होंने महसूस किया कि विदेशी भाषा जो उन दिनों सत्ता की भाषा थी, के माध्यम से देश के जन-मानस को नहीं जोड़ा जा सकता । 1916 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित होने वाले गांधी ने विरोध के बावजूद अपना वक्तव्य हिंदी में दिया। इसका इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ा कि 1918 में इंदौर में सम्पन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति गांधी को बनाया गया। इंदौर का उक्त अधिवेशन हिंदी प्रचार-प्रसार की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसी अधिवेशन में गांधी ने दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार की आवश्यकता पर ज़ोर दिया तथा धन संग्रह की अपील की। फिर क्या था – इंदौर के महाराजा यशवंत राव होल्कर तथा सेठ हुकुम चंद ने दस-दस हज़ार रुपए की सहायता राशि प्रदान की। वहीं यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तर भारत के कुछ युवक दक्षिण की भाषाओं को सीखने तथा हिंदी सिखाने के लिए दक्षिण के राज्यों में जाएँ तथा दक्षिण भारत के कुछ युवकों को हिंदी सीखने के लिए प्रयाग भेजा जाए।
गांधी की योजना तब रंग लाई जब 1918 में भारत सेवा संघ के युवकों ने गांधी से हिंदी प्रचारक भेजने की माँग की। तत्काल गांधी ने अपने 18 वर्षीय पुत्र श्री देवदास गांधी को हिंदी – प्रचार के लिए मद्रास भेजा । धीरे-धीरे 1927 में ‘दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा’ के रूप में एक स्वतंत्र संस्था का गठन कर दिया गया । आज भी यह राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है जो हिंदी प्रचार के कार्य में संलग्न है। सन् 1936 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन नागपुर में हुआ जिसमें गांधी ने हिंदी प्रचार समिति वर्धा के गठन का सुझाव दिया। बाद में उसका नाम ‘राष्ट्रभाषा प्रचार समिति’ कर दिया गया जिसका उद्देश्य दक्षिण को छोड़कर शेष हिंदीतर राज्यों में हिंदी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना था । इस राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के साथ 16 अंगभूत संस्थाएँ बनीं जो प्रदेश स्तर पर राष्ट्रभाषा का प्रसार करने लगीं। धीर-धीरे इन संस्थाओं की प्रेरणा से समस्त दक्षिण भारत हिंदी प्रचार के तीव्र आंदोलन का साक्षी बन गया।
स्वराज आंदोलनकारियों ने धीरे-धीरे हिंदी को समूचे राष्ट्र के कार्य- व्यवहार के लिए स्वीकार कर लिया। यह निर्णय राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत था, हिंदी सीखना और सिखाना राष्ट्रीय कर्म माना जाने लगा । धीरे-धीरे हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद मैसूर , हिंदी प्रचार परिषद बंगलोर, महाराष्ट्र राष्ट्राभाषा सभा पुणे, हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, केरल हिंदी प्रचार सभा तिरुअनंतपुरम, साहित्यानुशीलन समिति मद्रास तथा कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा धारवाड़ की स्थापना से हिंदी की लोकप्रियता दिनानुदिन बढ़ने लगी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लगभग ४० वर्षों तक इस राजनीतिक मंच की कार्य व्यवहार की भाषा अंग्रेज़ी थी किंतु धीरे-धीरे स्वराज के साथ-साथ ‘स्वभाषा’ का यक्ष प्रश्न भी उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। स्वराज के साथ-साथ राष्ट्रभाषा व राष्ट्र ध्वज भी किसी भी देश की अस्मिता की पहचान होते हैं। गांधी ने हिंदी की उस ताकत को बखूबी पहचान लिया था जो आज़ादी की लड़ाई में एकता का हथियार बनने की राह में चल पड़ी थी। उनका मानना था कि भारत की राजनीतिक आज़ादी व सांस्कृतिक स्वाधीनता हिंदी के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए वे हिंदी व देवनागरी दोनों की हिमायती थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा था कि यदि हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लिया जाए तो समाज में एकता सहज ही स्थापित हो सकती है। गांधी जी कहा करते थे कि यदि हिंदुस्तान की सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी हो जाय तो भाषाई एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और हिंदी सेतु का काम कर सकेगी। स्वराज की लड़ाई में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के सभी लोग हिंदी में बात करते थे। हिंदी स्वाधीनता की भाषा बनी, राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। गांधी अंग्रेज़ी को आधुनिकता की भाषा मानते थे किंतु ज्ञान की भाषा नहीं । उन्हें डर था कि अंग्रेजी के प्रति कहीं यह ललक गुलाम मानसिकता का शिकार न बना दे। गांधी घर के दरवाज़े-खिड़कियाँ खुली-रखना चाहते थे ताकि ताज़ा हवा आ सके किंतु हवाओं को आँधी बनने से रोकना भी चाहते थे। वे कहा करते थे कि जो बालक अपनी मातृभाषा के बजाय दूसरी भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हैं वे आत्महत्या करते हैं। विदेशी भाषा उन्हें अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित करती है । विदेशी भाषा माध्यम से अनावश्यक ज़ोर पड़ता है और मौलिकता तो नष्ट होती ही है तथा एक प्रकार का राष्ट्रीय संकट भी खड़ा होता है। मातृभाषा से इतर भाषा में शिक्षा देना उनके दिमाग को कुंद करना है। यह मातृद्रोह होगा। अपने देश की भाषाओं के महत्व को दर्शाने के क्रम में गांधी ने तुर्की के शासक कमालपाशा का उदाहरण दिया जिसने सत्ता सँभालते ही तुर्की को एक झटके से राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। कमालपाशा के इस उदाहरण से गांधी के हिंदी प्रेम और विवशता दोनों को देखा जा सकता है। काश! 1905 में बंगभंग के अवसर पर विदेशी शासन व वस्तुओं का बहिष्कार व स्वदेशी के प्रयोग का जो अखिल भारतीय आंदोलन चलाया गया उसी समय यदि विदेशी भाषा के वहिष्कार व स्वदेशी भाषा के प्रयोग का भी आंदोलन भी यदि शुरु कर दिया गया होता तो संभवत: आज भाषा की जटिल समस्या से हम जूझ न रहे होते।
आज राजनीतिक अधिनायकों और सामंतों ने राष्ट्रहित की चिंता छोड़ क्षणिक लाभ के लिए भारतीय जन-मानस को भाषाई दासता की बेड़ियों में जकड़ लिया है। हिंदी प्रचारकों ने जिस निष्ठा, लगन व संयम से हिंदी का प्रचार किया वह कल्पनातीत है। गांधी द्वारा भेजे गए हिंदी के प्रचारक अपनी पुस्तक, अपनी चटाई और अपनी लालटेन लेकर सुबह-सुबह किसी भी परिवार में दस्तक दे देते थे और आधा घण्टा हिंदी सिखाने के गांधी के संदेश को सुना देते थे। गांधी के इस अनुरोध को किसी परिवार ने कभी अस्वीकार नहीं किया। प्रचारक भी मंदिर, मस्जिद, विद्यालय या किसी सार्वजनिक स्थान पर, रुकते थे । वे किसी गृहस्थ के घर कभी नहीं रुकते थे। बदले में उन्हें पाँच रुपए महीने मानदेय दिया जाता था। आज यह बात कल्पना से भी बाहर की प्रतीत होती है । हिंदी का यह दुर्भाग्य रहा कि जिन राज्यों में लोगों ने बड़ी श्रद्धा- भावना के साथ हिंदी सीखी आज वहीं के लोग हिंदी – विरोधी स्वर देने लगे हैं । गांधी भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे हिंदी को नहीं। किंतु अंग्रेज़ी को तो कतई शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षधर नहीं थे । गांधी अंग्रेज़ी को क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में बाधक मानते थे । उनका मानना था कि जब तक अंग्रेज़ी रहेगी क्षेत्रीय भाषाओं में निकटता कभी नहीं आ सकती। गांधी कहा करते थे कि “राष्ट्रभाषा का यदि प्रचार करना है तो उसके लिए भगीरथ प्रयत्न करना होगा। आप लाटसाहब या सरकार के दरबार में जो प्रार्थना-पत्र भेजते हैं, तो किस भाषा में? यदि हिंदी में नहीं भेजते हैं तो लिखकर भेजिए। मैं कहता हूँ आप अपनी भाषा में लिखो। उनकी गरज होगी तो हमारी बात सुनेंगे।”
वैश्वीकरण के दौर में इस तथ्य को याद करना कई दृष्टियों से आवश्यक है कि भूमण्डलीकरण बाज़ार व्यवस्था का सार्वभौम रूप है। इसलिए यहाँ श्रम से नहीं धन से मनुष्य की पहचान की जाती है । इस स्थिति में आज हिंदी का प्रश्न बाज़ार की जरूरतों के संदर्भ में विचारणीय है तथा महात्मा गांधी ने भारत आने से पहले दक्षिण अफ़्रीका में रहनेवाले हिंदुस्तानियों के लिए सत्याग्रह किया था । मूलत: गुजराती भाषी व्यापारियों और हिंदी भाषी गिरमिटिया मज़दूरों के आपसी सम्पर्क का प्रश्न गांधी जी के सामने व्यावहारिक रूप में उपस्थित था। उन्होंने मजदूरों और व्यापारियों की एकता अंग्रेज़ी के माध्यम से नहीं कायम की, बल्कि इसके लिए उन्होंने हिंदी की अनिवार्यता को पहचाना । आगे चलकर 1909 में लंदन से अफ़्रीका वापस जाते समय पानी के जहाज़ पर उन्होंने अपनी ऐतिहासिक कृति ‘हिंद स्वराज’ लिखी। यह कृति साधारण पढ़े-लिखे लोगों को ध्यान में रखकर गुजराती में लिखी गई थी किन्तु अनेक भाषा-भाषी हिंदुस्तान में स्वराज्य की भाषा के रूप में उन्होंने हिंदी को जरूरी बताया था। इस तरह गांधी की दृष्टि में राष्ट्रभाषा पाने का अधिकार हिंदी को ही था।
गांधी जी के लिए भाषा का प्रश्न देश के भविष्य और समाज के उद्देश्य से अलग नहीं था। उन्होंने 1909 में ही यह बात कही थी कि अगर स्वराज्य मुट्ठी भर शिक्षितों का है तो सम्पर्क की भाषा अंग्रेज़ी होगी, लेकिन ‘यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों अनपढ़ लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताए हुए अस्पृश्य जनों के लिए है तो सम्पर्क भाषा केवल हिंदी ही हो सकती है’। दूसरे शब्दों में गांधी इस भूखी, निरक्षर जनता के हित और अधिकार को लेकर लड़ रहे थे, इसीलिए उन्होंने इन लोगों की अपनी भाषा को सम्पर्क-भाषा और राष्ट्रभाषा के रूप में परिभाषित किया। वे देख रहे थे कि अंग्रेज़ी माध्यम से शिक्षित नया कुलीन वर्ग हिंदी और भारतीय भाषाओं के बदले अंग्रेज़ी परस्त बनता जा रहा था । यह बात उन्हें कष्ट देती थी। उन्होंने राष्ट्रभाषा पर विचार करते हुए कहा था कि ‘जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं, वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं’।
यह बात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि गांधी जनता के प्रति विश्वासघात को देशद्रोह की श्रेणी में मानते थे । उनके लिए देश का अर्थ केवल कुछ भूभाग नहीं था, बल्कि उस भूमि और सीमा में रहनेवाली जीती-जागती मेहनतकश जनता था । आज के बाज़ारवादी दौर में गांधी जी की यह चिन्ता हमारे लिए अत्यन्त प्रासंगिक और विचारणीय बन गयी है। हम जानते हैं कि इस बाज़ारवादी संस्कृति के साथ अंग्रेज़ी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उस बाज़ार से लाभ उठानेवाला मध्यवर्ग अपनी भाषा छोड़कर अंग्रेज़ी की तरफ़ जा रहा है। गाँव में तथाकथित अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुल गए हैं जिनमें अंग्रेज़ी पढ़ाने वाले शिक्षक शायद ही शुद्ध अंग्रेज़ी बोल व लिख पाते होंगे लेकिन बाज़ार का आकर्षण इन स्कूलों की तरफ़ सबको आकर्षित कर रहा है। आज का माहौल ऐसा चिंताजनक है कि 1835 में जो ख्व़ाब मैकाले ने देखा था वह ब्रिटिश राज के रहते हुए उस तरह पूरा नहीं हुआ था जिस तरह आज के भूमण्डलीकरण के दौर में सम्भव हो रहा है। यहाँ ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव का कुछ अंश उधृत करना प्रासंगिक होगा –
“मैंने सम्पूर्ण भारत का दौरा किया और मैंने एक भी आदमी ऐसा नहीं देखा जो चोर हो, जो भिखारी हो । इस देश में मैंने ऐसी दौलत देखी, ऐसे उच्च नैतिक मूल्य और ऐसे योग्य लोग देखे कि मैं नहीं मानता कि हम कभी इस देश से जीत पायेंगे, जब तक कि हम इस देश की रीढ़ ही न तोड़ दें और इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम उसकी पुरानी और प्राचीन शिक्षा पद्धति, उसकी संस्कृति को बदल दें ताकि भारतीय यह सोचने लगें कि जो कुछ विदेशी और अंग्रेज़ी में है, वह अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ से श्रेष्ठ है, वे अपना स्वाभिमान, अपनी स्थानीय संस्कृति खो देंगे और वे वैसे बन जायेंगे जैसा हम चाहते हैं, एक वास्तविक पराधीन राष्ट्र”
मैकाले का यह स्वप्न आज पूरा होता दिख रहा है। गांधी के रहते उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता था। मैकाले के लिए भाषा का प्रश्न साम्राज्य के प्रभुत्व से जुड़ा हुआ था। अपने अहिंसक आंदोलनों के ज़रिए गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को हर स्तर पर चुनौती दी थी चाहे वह राजनीतिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो या सांस्कृतिक स्तर । उनके लिए स्वराज्य, स्वदेशी और स्वभाषा परस्पर जुड़े हुए थे। इसलिए गांधी विराट राष्ट्रीय विकल्प और स्वप्न प्रस्तुत कर सके । इसीलिए उन्होंने संसार के सबसे बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया । हम आज गांधी का नाम लेते हुए भी उनके इन आदर्शों को भुला चुके हैं। इसीलिए विदेशी पूंजी, विदेशी संस्कृति और विदेशी भाषा हम पर अपना वर्चस्व कायम करती जा रही है। यह कूबत गांधी में थी कि उन्होंने जुलाई 1928 के यंग इंडिया में लिखा था, “यदि मैं तानाशाह होता तो आज ही विदेशी भाषा में शिक्षा दिया जाना बन्द कर देता । जो आनाकानी करते, उन्हें बर्खास्त कर देता। मैं पाठ्य-पुस्तकों को तैयार किए जाने का इन्तज़ार नहीं करता।” लोकतन्त्र के प्रबल समर्थक गांधी केवल शिक्षा और भाषा के प्रश्न पर तानाशाह बनने की कामना करते हैं । आज अंग्रेज़ी भाषा और विदेशी शिक्षा जिस प्रकार भारत में अपना पाँव पसार चुकी है और उसके लिए जो घटिया तर्क दिए जा रहे हैं, उन्हें देखते हुए आज सचमुच गांधी जैसे ‘तानाशाह’ की एक बार फिर जरूरत महसूस की जा रही है।
गांधी जी की व्यवहारिक सूझ-बूझ अद्वितीय थी । वे उन बिंदुओं की पहचान करते हुए प्रस्ताविक करते थे जो जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र और आर्थिक भेदभावों को परेड के पीछे रखकर भारतीय जनता के बीच व्यापक एकता का आधार बन सकते थे। इसीलिए वे हिंदुस्तान के धनकुबेरों की आलोचना भी करते थे और स्वदेशी के विकास में उनकी सहायता भी लेने में भी समर्थ थे । दुर्भाग्य से आज व्यापारियों के हितों और श्रमजीवी जनता के हितों के बीच ऐसी दूरी हो गया है कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति या संगठन उनके बीच का साझा आधार नहीं पहचान पा रहा है जबकि राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से इस प्रकार का आधार खोजना आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब हम गांधी के नाम की माला जपने के बजाय उनकी शिक्षाओं से सही सीख लें । गांधी कुछ मुट्ठी भर शिक्षकों की जगह करोड़ों वंचितों को अपनी चेतना का मुख्य आधार मानते थे। वे अपने हर काम की कसौटी पर समाज के आखिरी जन को कसते थे। आज भी गांधी के इस आखिरी आदमी को इन करोड़ों गरीबों, निरक्षरों, दलितों , महिलाओं के हित के केंद्र में रखकर हम समाज के सभी स्तरों के बीच एकता की ज़मीन की खोज कर सकते हैं । लेकिन यह काम विदेशी भाषा में सम्भव नहीं है। गांधी की तरह सामाजिक, राजनीतिक उद्देश्य और भाषा के प्रश्न को आपस में जोड़ना पड़ेगा तथा इन सभी चीज़ों की कसौटी जनसाधारण को बनाना पड़ेगा।
आज इतना बदलाव जरूर दिख रहा है कि आज हमारे समाज में अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव के समानान्तर हिंदी अपने सामर्थ्य का भली प्रकार ज्ञान करा रही है। जो चैनल केवल अंग्रेज़ी प्रसारण का लक्ष्य लेकर आए थे, आज उनके हिंदी चैनलों की संख्या अंग्रेज़ी चैनलों से ज़्यादा है। जो टेलीविजव चैनल हिंदी के प्रयोग को अछूत समझते थे, आज उनका यह संकल्प पता नहीं कहाँ खो गया है और जनसरोकारों से सम्पन्न हिंदी अपनी जगह यथावत है। कल तक विज्ञापनों की भाषा अंग्रेज़ी हुआ करती थी, अंग्रेज़ी के विज्ञापन निर्माताओं को बाज़ार में यश और धन की प्राप्ति होती थी किन्तु आज स्थिति बदल गयी है । सबसे प्रतिभाशाली मस्तिष्क हिंदी के विज्ञापनों से संलग्न हैं । सबसे लोकप्रिय, मौलिक,प्रभावशाली और कलात्मक अभिव्यक्तियाँ हिंदी विज्ञापनों में दृष्टिगोचर होती हैं। मालिकों की भाषा अंग्रेज़ी है। वे अंग्रेज़ी के प्रभुत्व के लिए पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन उपभोक्ता की भाषा हिंदी है इसलिए उन्हें अपना भाषा अहंकार छोड़कर हिंदी के आगे नतशिर होना पड़ता है। क्योंकि हिंदी भाषी मध्यवर्ग बड़े पैमाने पर बाज़ार में हिस्सेदारी कर अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है।
हमारी धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता की पहचान हिंदी से जुड़ी हुई है। इस हिंदी का विरोध धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता का विरोध है। कम्प्यूटर के लिए भाषा की जिस पद्धति का आधार लिया गया है, वह शून्य की अवधारणा भारत है और वह भी उसी हिंदी प्रदेश की जिसकी सांस्कृतिक परम्परा ऋग्वेद और हड़प्पा के काल से 21वीं सदी के बाजारीकरण के दौर तक सतत चली आ रही है । हमारे इस सांस्कृतिक अविच्छन्न प्रवाह को गांधी जी ने सबसे पहले हिंद स्वराज में बड़े गौरवपूर्ण शब्दों में प्रस्तुत किया था। संस्कृति, भाषा और गणना पद्धति आदि सभी बातें आपस में जुडी हुई हैं। शून्य और एक के सूत्र से कम्प्यूटर की भाषा का विकास इस आवश्यकता को उजागर करता है कि भविष्य में रोमन की जगह नागरी नये संचार माध्यम का रूप लेगी और भाषा वैज्ञानिक भी इस आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं । गांधी इस भविष्य को तो नहीं देख रहे थे, लेकिन इतिहास से सीख कर उन्होंने जो अवधारणाएँ दीं उनका तर्कसंगत विकास करके हम आज की इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की में वहाँ के तानाशाह कमालपाशा में यही अन्तर है। जहां कमालपाशा अपनी संस्कृति और उस संस्कृति की पहचान – लिपि – को मिटा रहे थे वहीं गांधी ऐसे तानाशाह बनना चाहते थे, जो अपनी महान संस्कृति और उसकी पहचान को जनता के से तथा उसकी भाषा और लिपि से जोड़ने का प्रयास कर रहे थे।
गांधी अंग्रेज़ी भाषा के दुश्मन नहीं थे। अपनी भाषा की उपेक्षा की कीमत पर अंग्रेज़ी का प्रभुत्व इन्हें स्वीकार्य नहीं था। वे कहते थे, “यदि विदेशी भाषाएँ और संस्कृति मेरे घर को सुगंधित करें तो मैं विदेशी समीर के लिए अपनी खिड़कियाँ खोल दूंगा । किंतु यदि वे तूफ़ान बनकर मेरे घर को उखाड़ना चाहेंगी तो मैं चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊँगा” गांधी अंग्रेज़ी शिक्षा पद्धति और शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेज़ी के प्रयोग को राष्ट्र के खिलाफ़ मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेज़ी शिक्षा भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना देगी, नकलची बना देगी। स्वाभाविक प्रतिभा का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेज़ी होने से जनता से संबंध विच्छेद हो जाएगा जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होगी। जनता की भाषा और सत्ता की भाषी में एकरूपता होने से ही सही अर्थों में स्वराज की प्राप्ति होगी। अंग्रेज़ी जानने वाले भारतीय ही प्रजा को गुलाम बनाकर रखेंगे। प्रजा की हाय अंग्रेज़ों पर नहीं अंग्रेज़ीदाँ भारतीयों को लगेगी, ऐसा गांधी का मानना था। भारत के स्वतंत्र होने पर बी.बी.सी. संवाददाता ने गांधी की प्रतिक्रिया अंग्रेज़ी में जाननी चाही तो गांधी ने दो टूक शब्दों में कहा था कि ‘गांधी अंग्रेज़ी भूल गया है।’ यह गांधी का स्वदेश और स्वभाषा प्रेम था।
गांधी सहज सरल हिंदी के पक्षधर थे। वे हिंदी को हिंदुस्तानी कहते थे। वे कहते थे कि “हिंदी उस भाषा का नाम है जिसे हिंदू और मुसलमान कुदरती तौर पर बगैर प्रयत्न के बोलते हैं । हिंदुस्तानी और उर्दू में कोई अंतर नहीं है। देवनागरी में लिखी जाने पर वह हिंदी और फारसी लिपि में लिखी जाने पर वह उर्दू हो जाती है”।उन्होंने हिंदी उर्दू के बीच की आम भाषा को हिंदुस्तानी कहा और उसी को स्वीकारने की वकालत थी।
गांधी प्रांतीय संकीर्णता को छोड़कर सभी भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि अपनाने की वकालत भी की। मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि मानने वाले गांधी तमाम लिपियों के अनावश्यक बोझ से मुक्ति चाहते थे। वे अंग्रेजों से भी निर्भीक होकर कहते थे कि “हिंदुस्तान की आम भाषा अंग्रेज़ी नहीं बल्कि हिंदी है, वह आपको सीखनी होगी और हम तो आपसे अपनी भाषा में ही व्यवहार करेंगे।“
उनका स्पष्ट मत था कि सभी भारतीयों को उनकी अपनी-अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा दी जानी चाहिए तथा समस्त भारतीय पारस्परिक बोलचाल के किए हिंदी का प्रयोग करें। वे अंतरराष्ट्रीय व्यवहार के लिए अंग्रेज़ी भाषा को भी अनुचित नहीं मानते थे। उनकी यह भी मान्यता थी कि राष्ट्रभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र का निर्माण सम्भव नहीं है। बिना राष्ट्रभाषा के राष्ट्र गूँगा बनकर रह जाता है। अत: वे अंग्रेज़ी के प्रभुत्व से देश को मुक्त करना चाहते थे जो शायद हो न सका। आज गांधी फिर एकबार प्रासंगिक हो गए हैं । अब एकबार फिर वक्त आ गया है कि हम गांधी की भाषा दृष्टि, उनके विचार तथा उनके साहस का सहारा ले स्वतंत्र भारत की भाषाई अस्मिता को सकारात्मक ढंग से प्रस्तुत कर अतीत की ऐतिहासिक भूलों का परिमार्जन करें।
Last Updated on November 28, 2020 by srijanaustralia
- प्रो. विनोद कुमार मिश्र
- महासचिव
- विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस
- [email protected]
- विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरिशस